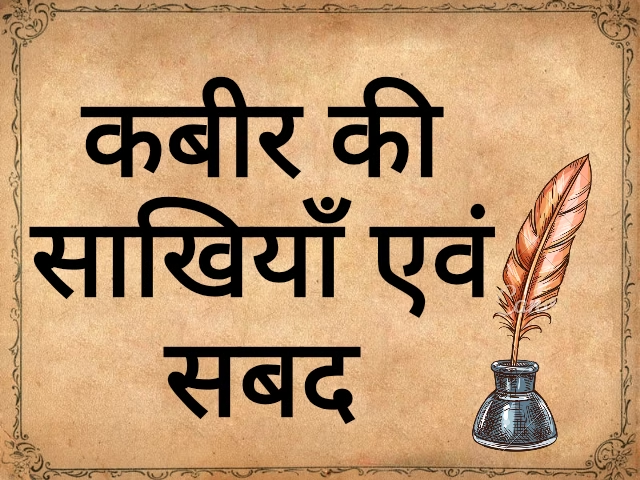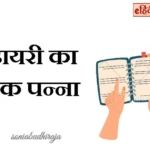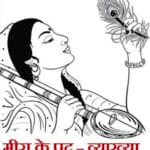NCERT Study Material for Class 9 Hindi Kshitij Ch - 9 Kabir ki Sakhiyan evam Sabad
NCERT Study Material for Class 9 Hindi Kshitij Chapter- 9 Kabir – Sakhiyan evam Sabad (Kabir ki sakhiyan evam Sabad)
हमारे ब्लॉग में आपको NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 (Course A) की हिंदी पुस्तक ‘क्षितिज’ के पाठ पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर स्पष्ट एवं सरल भाषा में प्राप्त होंगे। साथ ही काव्य – खंड के अंतर्गत निहित कविताओं एवं साखियों आदि की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है।
यहाँ NCERT HINDI Class 9 के पाठ – 9 ‘कबीर – साखियाँ एवं सबद’ की व्याख्या दी जा रही है।
यह व्याख्या पाठ की विषय-वस्तु को समझने में आपकी सहायता करेगी। इसे समझने के उपरांत आप पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकेंगे। आशा है यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
NCERT Class 9 Hindi Kshitij Chapter – 9 कबीर – साखियाँ एवं सबद (कबीर की साखियाँ एवं सबद)
Table of Contents
Kabir ki Sakhiyan evam Sabad - Explanation
कबीर की साखियाँ एवं सबद - सहायक सामग्री
मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहिं।
मुकताफल मुकता चुगैं, अब उड़ि अनत न जाहिं । 1।
शब्दार्थ –
- मानसरोवर – पवित्र तालाब (मन रूपी सरोवर अर्थात् हृदय)
- सुभर – अच्छी तरह भरा हुआ
- हंसा – हंस पक्षी (जीव)
- केलि- क्रीड़ा, खेल
- मुकताफल – मोती (प्रभु भक्ति)
- मुक्त – मुक्त होकर (स्वछंद होकर)
- अनत – किसी और जगह
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। इसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात् हंस इस आनंददायक वातावरण में खुश हैं। इस स्वच्छ जल से भरे सरोवर में वे स्वतंत्र होकर अनमोल मोती चुग रहे हैं इसलिए अब वे कहीं और नहीं जाना चाहते।
भावार्थ –
प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने भक्तों के लिए प्रभु की भक्ति को अनमोल बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब प्रभु की भक्ति रूपी स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा होता है तब हंस रूपी जीव उस सरोवर में प्रभु भक्ति के कारण आनंदित होते हैं। वे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु की भक्ति रूपी मोती को ग्रहण करते हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्य किसी और स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं।
प्रेमी ढूँढ़ मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोइ।
प्रेमी कौं प्रेमी मिलै, सब विष अमृत होइ। 2।
शब्दार्थ –
- प्रेमी – प्रेम करने वाला प्रभु का भक्त
- मैं – स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अहंकार
- विष – बुरे भाव (विकार)
- अमृत – ज्ञान
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझकर अपने समान प्रभु से प्रेम करने वाले भक्त को ढूँढ़ रहा था लेकिन मुझे कोई अन्य भक्त नहीं मिला। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिला तो प्रभु सत्संग से मन की सभी बुरी भावनाएँ नष्ट हो गई और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हुआ।
भावार्थ –
भाव यह है कि जब है स्वयं को प्रभु का सबसे बड़ा भक्त मानकर प्रभु का भक्त ढूँढ़ रहा था तब मुझे कोई भक्त नहीं मिला लेकिन जब मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चा ईश्वर भक्त बना तब मुझे सच्चा ईश्वर भक्त मिल गया। उसके मिलने से हमारे बीच निरंतर प्रभु चर्चा, प्रभु सत्संग के कारण हमारे मन की सभी दुर्भावनाएँ दूर हो गई और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हुआ। अतः कबीरदास जी अहंकार को प्रभु भक्त और प्रभु भक्ति दोनों के मिलने में बाधक मानते हैं।
हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारि।
स्वान रूप संसार है, भूँकन दे झख मारि। 3।
शब्दार्थ –
- हस्ती – हाथी (ज्ञान)
- सहज – सहज साधना (आडंबर रहित / बिना दिखावे की भक्ति)
- दुलीचा डारि – कालीन बिछाना (अपनी स्थिति को मज़बूत करना)
- स्वान – कुत्ता
- भूँकन दे – भौंकने दो
- झख मारि – समय बर्बाद करते हुए
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी साधकों से कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर अपनी साधना को सुदृढ़ (मज़बूत) करने का निरंतर प्रयास करते रहो। यह संसार तुम्हें सुमार्ग पर चलते देख, अपने मन में स्वयं को छोटा मानकर कुत्ते के समान तुम पर भौंकेगा परंतु तुम उनक भौंकने पर ध्यान न देना। वह स्वयं ही अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएगा।
भावार्थ –
कबीर दास जी के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला साधक संसार की विषय वासनाओं (बंधनों) से ऊपर उठ जाता है इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले साधक को उन्होंने हाथी पर सवार कहा है । कबीरदास जी हाथी पर सवार साधक को अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले साधक को भक्त के रूप में अपने स्थान को मज़बूत करने के लिए उसे नियमित रूप से आडंबर रहित साधना करने की सलाह देते हैं।
जिस प्रकार विशालकाय हाथी को मार्ग से गुज़रता देख कुत्ते बिना कारण उस पर भौंकते हैं उसी प्रकार साधक को उसका नियम धर्म करते देख संसार के लोग उसकी निंदा करते हैं। कबीर दास जी ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देने को कहते हैं। ऐसे लोग बोल-बोल कर स्वयं ही चुप हो जाते हैं इसलिए साधक को केवल अपने प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए।
पखापखी के कारनै, सब जग रहा भुलाना।
निरपख होइ के हरि भजै, सोई संत सुजान। 4।
शब्दार्थ –
- पखापखी – पक्ष – विपक्ष (किसी को सही और किसी को गलत मानना)
- कारनै – कारण
- निरपख – निष्पक्ष
- सुजान – ज्ञानी, चतुर
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपने संप्रदाय का पक्ष लेकर अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ (बेहतर) मानते हैं। वह अपने धर्म का समर्थन तथा दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। इसी पक्ष-विपक्ष के चक्कर में पड़ कर संसार अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। जो व्यक्ति धर्म और संप्रदाय में पड़े बिना अर्थात् निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
भावार्थ –
भाव यह है कि धर्म और जाति के भेदभाव के कारण सारा संसार ईश्वर की भक्ति को भूल गया है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन करता है कबीरदास जी के अनुसार, वही सच्चा भक्त है।
हिंदू मूआ राम कहि, मुसलमान खुदाइ।
कहै कबीर सो जीवता, जो दुहुँ के निकट न जाइ। 5।
शब्दार्थ –
- मूआ- मर गया
- जीवता – जीवित रहता है
- दुहुँ – दोनों
शाब्दिक अर्थ –
हिंदू राम का नाम जपते हुए तथा मुसलमान खुदा का नाम लेते हुए मर मिटे।वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे अर्थ में जीवित रहता है।
भावार्थ-
कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को धर्म और जाति में सीमित करके प्रभु की भक्ति करता है और बिना सच्ची भक्ति को प्राप्त किए उसका जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु जो धार्मिक बंधनों से ऊपर उठकर प्रभु को हर जीव में देखता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्म लेकर अपने उद्देश्य को पूरा करने के कारण वह सही मायने में जीवित कहलाता है।
काबा फिरि कासी भया, रामहिं भया रहीम।
मोट चून मैदा भया, बैठिए कबीरा जीम।6।
शब्दार्थ –
- काबा – मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल
- कासी – काशी, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल
- मोट – मोटा
- चून – आटा
- जीम – भोजन करना
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं राम – रहीम, हिंदू – मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तब मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। अपनी संकीर्ण (छोटी) सोच के कारण मैं जिस मोटे आटे को खाने योग्य नहीं समझ रहा था अब वही बारीक मैदे के समान हो गया है जिसे मैं सरलता से खा रहा हूँ।
भावार्थ-
भाव यह है कि जैसे ही मेरे मन से अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने की भावना समाप्त हो गई वैसे ही सभी धर्मों के ईश्वर और तीर्थ स्थल मेरे लिए एक समान हो गए। अब हर जगह ईश्वर प्राप्ति के कारण मैं ईश्वर भक्ति का रस (आनंद) ले पाता हूँ।
ऊँचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊँच न होइ।
सुबरन कलस सुरा भरो, साधू निंदा सोई। 7।
शब्दार्थ –
- जनमिया – जन्म लेकर
- करनी – कर्म
- सुबरन – सोने का
- कलस – कलश, घड़ा
- सुरा – मदिरा (शराब)
- निंदा – बुराई
- सोई – उसकी
शाब्दिक अर्थ –
कबीरदास जी कहते हैं कि ऊँचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति महान या सम्मान योग्य नहीं बन जाता है। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अपनी इसी बात को उदाहरण द्वारा समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सोने के पवित्र पात्र में मदिरा भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं।
भावार्थ-
कर्मों के महत्त्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊँचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते वह अपने कर्मों द्वारा ऊँचे कुल का नाश कर देता है।
सबद (पद)
(1) मोकों कहाँ ढूँढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में।
ना तो कौने क्रिया-कर्म में, नहीं योग बैराग में।
खोजी होय तो तुरतै मिलिहौं, पल भर की तालास में।
कहैं कबीर सुनो भई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में।।
शब्दार्थ –
- मोकों – मुझे
- बंदे – मनुष्य, इंसान
- देवल – मंदिर
- कौने – किसी प्रकार के
- क्रिया – कर्म – बाहरी आडंबर (पूजा की विभिन्न विधियाँ)
- योग – कठिन साधना
- बैराग – वैराग्य (गृह त्याग)
- खोजी – ढूँढ़ने वाला (सच्चा भक्त)
- तालास – तलाश
शाब्दिक अर्थ –
प्रस्तुत सबद (पद) में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सदैव मनुष्य के समीप ही रहता है परंतु मनुष्य उसे पाने के लिए भटकता रहता है। ईश्वर न तो मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न ही काबा और कैलाश आदि तीर्थ स्थलों में जाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। न किसी प्रकार के दिखावे से पूर्ण पूजा की विधि से ईश्वर मिलता है और ना ही कठिन योग और वैराग्य से। सच्चे भक्तों को पलभर की तलाश में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि ईश्वर तो सभी जीवो में श्वास रूप में विद्यमान है अर्थात् हर प्राणी में ईश्वर का वास है।
भावार्थ –
प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध कर मनुष्य के भीतर ही ईश्वर के व्याप्त होने का संकेत दिया है। उनके अनुसार ईश्वर सभी जीवों में जीवन के रूप में अर्थात् आत्मा के रूप में विद्यमान है इसीलिए उसे पाने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
(2) संत भाई आई ग्याँन की आँधी रे।
भ्रम की टाटी सबै उड़ाँनी, माया रहै न बाँधी।।
हिति चित्त की द्वै थूँनी गिरौंनी, मोह बलिंडा तूटा।
त्रिस्नाँ छाँनि परि घर ऊपरि, कुबधि का भाँडाँ फूटा।।
जोग जुगति करि संतौँ बाँधी, निरचू चुवै न पाँणी ।
कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाँणी।।
आँधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीनाँ ।
कहै कबीर भाँन के प्रगटे उदित भया तम खीनाँ।
शब्दार्थ –
- ग्याँन – ज्ञान
- टाटी – परदे के लिए लगाए हुए बॉंस आदि की पट्टियों का पल्ला, कच्ची दीवार
- हिति – स्वार्थ
- चित्त – इच्छा
- थूँनी – स्तंभ, खंभा
- गिराँनी – गिर गया
- बलिंडा – छप्पर की मज़बूत मोटी लकड़ी
- त्रिस्नाँ – तृष्णा, लालच
- छाँनि – छप्पर
- कुबधि – अज्ञान (मन के विकार)
- भाँड़ा फूटा – भेद खुला
- निरचू – थोड़ा भी
- चुवै – रिसता है, टपकता है
- बूठा – बरसा
- भींनाँ – भीग गया
- तम – अंधकार
- खीनाँ – क्षीण हुआ, छट गया
शाब्दिक अर्थ –
प्रस्तुत सबद में कबीरदास जी ने ज्ञान की आँधी के रूप के माध्यम से ज्ञान के महत्त्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हे संतों! हे प्रभु भक्तों! ज्ञान की आँधी आ गई है। इस ज्ञान की आँधी के आने से भ्रम रूपी दीवारें गिर गईं हैं और सांसारिक सुख अर्थात् माया रूपी बंधन खुल गए हैं। स्वार्थ और इच्छा रूपी दो स्तंभ (खंभे) ज्ञान की आँधी के कारण गिर गए हैं। बाँस की मोटी लकड़ी, जिस पर छप्पर टिका होता है वह भी टूट गया।
भ्रम, माया, स्वार्थ और इच्छाओं के नष्ट हो जाने पर लालच रूपी छप्पर (छत) भी हट गया है । जिस प्रकार झोपड़ी की छत हट जाने पर उसमें रहने वालों की वास्तविक स्थिति, संसार के सामने आ जाती है उसी प्रकार ज्ञान की आँधी आने पर मनुष्य को अपने मन की दुर्बलताओं का पता चलता है। जिनका घर मज़बूत होता है अर्थात् जो साधु स्वभाव के होते हैं, उनके घर पर इस आँधी का ज़रा – सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रभु की महिमा का ज्ञान होने लगता है तब माया,मोह, कपट रूपी कूड़ा (बुरे भाव) निकल जाने से, मनुष्य का मन साफ़ हो जाता है।
जैसे आँधी के बाद वर्षा आने पर सारी धूल साफ़ हो जाती है और व्यक्ति को सब स्पष्ट दिखाई देता है वैसे ही ज्ञान की आँधी के बाद मनुष्य को प्रभु से अपने संबंध का ज्ञान होता है और वह प्रभु के प्रेम में पूरी तरह भीग जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस ज्ञान के प्रकट होने पर सारा अंधकार हट जाता है और मन पाप रहित होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है।
भावार्थ –
भाव यह है कि जिस प्रकार आँधी चलने पर कमज़ोर झोपड़ियों की छत, दीवारें आदि टूट कर गिर जाती हैं उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य के मन से लोभ, मोह, माया आदि कमज़ोर भाव नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की आँधी के बाद वर्षा जल रूपी प्रभु के प्रेम में भीगकर मनुष्य प्रभु – भक्ति में लीन हो जाता है।