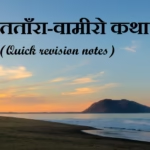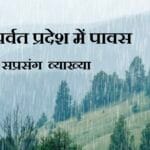NCERT Study Material for Class 10 Hindi Sparsh Chapter 4 - Manushyata composed by Maithili Sharan Gupt
हमारे ब्लॉग में आपको NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10 (Course B) की हिंदी पुस्तक ‘स्पर्श’ के पाठ पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर स्पष्ट एवं सरल भाषा में प्राप्त होंगे।
साथ ही काव्य – खंड के अंतर्गत निहित कविताओं एवं साखियों आदि की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है।
यहाँ NCERT Class 10 Hindi के पाठ – 4 ‘मनुष्यता’ की व्याख्या दी जा रही है। यह कविता राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है।
यह व्याख्या पाठ की विषय-वस्तु को समझने में आपकी सहायता करेगी। इसे समझने के उपरांत आप पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकेंगे। आशा है यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
Table of Contents
Manushyata - मनुष्यता
शब्दार्थ एवं सप्रसंग व्याख्या
विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी¸
मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करे सभी।
हुई न यों सु–मृत्यु तो वृथा मरे¸ वृथा जिये¸
मरा नहीं वहीं कि जो जिया न आपके लिए।
यही पशु–प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे¸
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- मर्त्य – मरणशील (जिसका नष्ट होना निश्चित है)
- सुमृत्यु – मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति को उसके अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाए, उसकी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है।
- वृथा – व्यर्थ (बेकार)
- पशु-प्रवृत्ति – पशु जैसा अमानवीय स्वभाव
- चरे – पेट भरे
प्रसंग –
प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है।
व्याख्या –
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी संपूर्ण मनुष्य जाति को (संबोधित करते हुए) कहते हैं कि तुम इस बात पर विचार करो कि तुम्हें मनुष्य के रूप में मिला यह शरीर, यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है अर्थात् मरणशील है। मृत्यु एक – न- एक दिन आएगी ही इसीलिए मृत्यु से मत डरो।
गुप्त जी कहते हैं कि तुम अपना यह जीवन इस प्रकार जियो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी संसार तुम्हें याद रखें और तुम्हारी मृत्यु, मृत्यु नहीं सुमृत्यु बन जाए। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी तुम दूसरों का हित (भलाई) के बारे में नहीं सोचोगे तो संसार तुम्हें याद नहीं करेगा ऐसी स्थिति में तुम्हारा मरना भी व्यर्थ है और तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है।
कवि यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है अर्थात् दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वह कभी नहीं मरता। अपने सद्गुणों के कारण वह अमर हो जाता है। कवि मनुष्य और पशु में अंतर बताते हुए कहते हैं कि पशु केवल अपने हिस्से का चर कर (खाकर) अपना पेट भरता है। परंतु केवल मनुष्य में ही यह गुण है कि वह अपने साथ-साथ औरों के लिए भी कुछ करने में समर्थ है। अतः मनुष्य होकर भी केवल अपने लिए सोचना अमानवीयता (पशु जैसा स्वभाव) है। मनुष्य वही है जो मानवीय गुणों से संपन्न है अर्थात् जिसका हृदय परोपकार की भावना से भरा है।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती¸
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती;
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखण्ड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे¸
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे।।
शब्दार्थ –
- उदार – दयालु / दानशील
- धरा – धरती
- कृतार्थ – आभारी
- कीर्ति – यश
- कूजती – गुणगान करना
- अखंड – जो तोड़ा नहीं जा सकता / जुड़ा हुआ
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में गुप्त जी बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के भले के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, संसार में युगों – युगों तक उनका गुणगान किया जाता है।
व्याख्या – गुप्त जी कहते हैं कि दूसरों का भला करने के वाले और अपने मन में दया का भाव रखने वाले मनुष्यों का सदा गुणगान होता है। पुस्तकों में उनका बखान किया जाता है। ऐसे ही उदार (दानशील) मनुष्यों का धरती भी आभार मानती हैं। दूसरों की भलाई के लिए सदा कार्यशील रहने वालों का संसार में यश गाया जाता है।
अपनी कविता के माध्यम से गुप्त जी यह बताना चाहते हैं कि दूसरों का हित करने वालों के उपकार को संसार कभी नहीं भूलता उनकी कीर्ति यश की कहानियाँ लोगों द्वारा सदा पढ़ी और सुनाई जाती हैं। संसार उनके उदात्त (अच्छे) गुणों के कारण उनकी पूजा करता है। गुप्त जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को एकता और भाईचारे की भावना से बाँधता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है अर्थात् मनुष्य वही है जो सबको एकता के सूत्र में बाँधे और दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें।
क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी,
तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी।
उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया,
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर-चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे?
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- क्षुधार्त – भूख से व्याकुल
- करस्थ – हाथ में पकड़ा हुआ /लिया हुआ
- परार्थ – दूसरों के लिए
- अस्थिजाल – हड्डियों का समूह
- क्षितीश – राजा
- स्वमांस – अपने शरीर का मांस
- सहर्ष – प्रसन्नता (खुशी) से
- चर्म – चमड़ी
- अनित्य – सदा न रहने वाली
- अनादि – सदा रहने वाला
काव्यांश में वर्णित पौराणिक पात्रों के प्रसंग : –
(केवल छात्रों की जानकारी के लिए)
* रंतिदेव – रंतिदेव बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंतिदेव जब भी किसी गरीब को कष्ट में देखते थे। अपना सर्वस्व दान कर देते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ा था तब रंतिदेव ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। रंतिदेव स्वयं 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे।
भूख – प्यास के कारण राजा का शरीर काँपने लगा था। 49 वें दिन उन्हें कहीं से भोजन मिला। उन्होंने भोजन का निवाला हाथ में लिया ही था कि एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके सामने आ गए। रंतिदेव ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन दिया।शेष भोजन अपने परिवार को देना चाहा, परंतु एक शूद्र अतिथि याचक उनके द्वार पर आ गया राजा ने अन्न उसको भी दे दिया। तब अतिथि बोला कि उसका कुत्ता भी भूखा है, इसलिए उसके लिए अन्न चाहिए। राजा ने बचा हुआ अन्न शूद्र अतिथि को दे दिया।
अन्न समाप्त हो जाने के बाद राजा के पास केवल इतना ही पानी बचा था कि किसी एक व्यक्ति की प्यास बुझ सके, वह जल ग्रहण करने वाला ही था कि चांडाल की दीन करुण याचना सुनी। राजा ने जल उस चांडाल को दे दिया. राजा ने प्रार्थना कि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सभी प्राणियों की रक्षा हो, उनके सभी कष्ट मैं भोग लूँगा. तभी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा रंतिदेव के समक्ष प्रकट हो गए। राजा रंतिदेव का संयम, धैर्य व परोपकारिता देखकर तीनों देव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा व उसके परिवार को मोक्ष प्रदान किया।
* दधीचि – एक बार वृत्रासुर नाम के राक्षस ने इंद्र देव को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने वृत्रासुर का अंत ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से ही होने की बात कही। ब्रह्माजी की बात सुन देवराज इंद्र झिझकते हुए ऋषि दधीचि के पास पहुँचे। जब उन्होंने वज्र के लिए ऋषि से उनकी हड्डियों की आवश्यकता की बात कही तो वे प्रसन्नता से देने को तैयार हो गए।
अपनी हड्डियों का दान कर उन्होंने इसके बाद योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। जिसके बाद उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस तरह ऋषि दधीचि दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर अमर दानी बन गए।
* उशीनर – उशीनर के राजा शिवि बहुत दानी थे। शिवि के दान धर्म की कथा देवतागण स्वर्गलोक में भी सुनाया करते थे।एक बार इंद्र और अग्नि ने शिवि की दानशीलता की परीक्षा लेने की सोची।अग्निदेव ने कबूतर का रूप धरा और इंद्र ने बाज़ का। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए उड़ता हुआ शिवि की गोद में पहुँचा और प्राणरक्षा की प्रार्थना की। शिकार का पीछा करता इंद्र के रूप में बाज़ भी वहाँ आ पहुँचा। जब बाज़ ने राजा से अपना शिकार माँगा तब राजा ने कहा कि वह अपनी शरण में आए इस कबूतर को उसे नहीं सौंप सकते।
इंद्ररूपी बाज़ ने कहा कि यदि आप कबूतर को नहीं छोड़ना चाहते तो इसके वज़न के बराबर अपना मांस काटकर दे दीजिए। राजा ने एक-एक करके अपने सभी अंगों का मांस काटकर तराज़ू पर रख दिया तो भी वह कबूतर के वज़न के बराबर न हुआ। तब राजा शिवि कबूतर की जान बचाने के लिए खुद तराज़ू के पलड़े में बैठ गए। ऐसा करते ही कबूतर और बाज़ दोनों अपने असली रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवों ने राजा की प्रशंसा की और उन्हें स्वस्थ कर दिया। देवों ने वरदान दिया कि जब भी शरणागत की रक्षा करने वालों, प्रजापालक व धर्मरक्षक वीरों का जिक्र होगा, शिवि का नाम सुनकर देवता भी प्रशंसा में सिर झुकाएँगे।
* कर्ण – सूर्य पुत्र कर्ण वीर योद्धा होने के साथ – साथ दानवीर भी थे। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलिभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता है।
कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण हर रोज़ लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता था। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। तब देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके शरीर के कवच और कुंडल दान में माँग लिए. इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण ने एक पल का समय गँवाए बिना स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए।
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्तजी ने पौराणिक कथाओं के महान पात्रों के उदाहरण देकर परोपकार के लिए उनके द्वारा किए गए त्याग का वर्णन किया है।
व्याख्या – कवि दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले दानवीरों का बखान करते हुए कहते हैं कि 48 दिन से भूख से व्याकुल परम दानी राजा रंतिदेव ने स्वयं भूखे रहकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन से भरा हुआ थाल दूसरों में बाँट दिया और देवताओं के हित के लिए दानवीर ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। जिससे उनकी हड्डियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण हुआ और देवताओं को सताने वाले राक्षस वृत्रासुर का वध किया जा सका।
उशीनर (गंधार देश) के राजा शिवि ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। दानवीर कर्ण ने इंद्र के माँगने पर अपने शरीर का कवच उन्हें प्रसन्नता से दान कर दिया। यह जानते हुए भी कि यह कवच युद्ध में उसकी रक्षा करेगा, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा।
कवि कहते हैं कि सदा न रहने वाले इस शरीर के लिए मनुष्य क्यों डरता है अर्थात् मनुष्य को इस शरीर का मोह क्यों है? मनुष्य तो तभी अमर हो सकता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और दूसरों के हित के लिए जो अपने प्राण तक न्योछावर कर दे सच्चे अर्थों में वही मनुष्य कहलाता है।
सहानुभूति चाहिए¸ महाविभूति है वही;
वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
विरूद्धवाद बुद्ध का दया–प्रवाह में बहा¸
विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा?
अहा! वही उदार है परोपकार जो करे¸
वहीं मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- महाविभूति – बड़ी पूँजी (संपत्ति)
- वशीकृता – वश में कई हुई
- मही – धरती
- विरुद्धवाद – महात्मा बुद्ध ने अपने हृदय में करुणा के कारण लोगों की भलाई के लिए अपने समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था जिसे विरुद्धवाद कहा जाता है।
- विनीत – विनम्र / विनय युक्त
- परोपकार – दूसरों की भलाई
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए यह कहते हैं कि करुणा मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी है और यह करुणा मनुष्य को समाज में बड़े से बड़े परिवर्तन लाने की शक्ति देती है।
व्याख्या – प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव है, वह धनी है। दूसरों के दुख का अनुभव करना मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी (संपत्ति) है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वालों के सामने तो सारी धरती नतमस्तक होती है। यह संपूर्ण पृथ्वी अपने – आप ही उसके वश में हो जाती है।
कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दूसरों के दुख को समझने वाले और प्राणी मात्र के प्रति करुण भाव रखने वाले महात्मा बुद्ध ने सभी प्राणियों की भलाई के लिए उस समय में प्रचलित अनेक रीतियों (नियमों) का विरोध किया। लोगों के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए परिवर्तन से सारा संसार उनके सामने विनम्र होकर झुक गया। यह मनुष्य के हृदय में रहने वाले करुणा के भाव का प्रभाव है जो उसे पुरानी मान्यताओं और समाज का विरोध करने की शक्ति देता है।
कवि कहते हैं कि जिस हृदय में दूसरों के लिए करुणा है, दया है, जो परोपकारी है और जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों तक को त्याग देता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है।
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में,
सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में|
अनाथ कौन हैं यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं,
दयालु दीनबन्धु के बड़े विशाल हाथ हैं|
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- मदांध – घमंड में अंधा
- तुच्छ – महत्त्वहीन / छोटा
- वित्त – धन-संपत्ति
- दीनबंधु – दीनों (गरीबों) की सहायता करने वाले
- अतीव – बहुत
- अधीर – बेचैन
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी मनुष्य को यह समझा रहे हैं कि धन और वैभव प्राप्त होने की स्थिति में मनुष्य को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए।
व्याख्या – कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भूल कर भी धन-संपत्ति जैसे छोटे साधनों के गर्व में अंधा नहीं होना चाहिए अर्थात् कभी भी नष्ट हो जाने वाले रुपये – पैसे के कारण अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वयं को धन का स्वामी समझकर हृदय में घमंड करना व्यर्थ है। मनुष्य को सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि धन होने से कोई व्यक्ति धनहीन (गरीब व्यक्ति) का स्वामी नहीं बन जाता।
इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी अर्थात् सब का पालन करने वाले ईश्वर ही सब जीवों के स्वामी हैं और उनके हाथ बहुत विशाल हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर परम दयालु हैं और दीन – दुखियों की सहायता करते हैं। आशीर्वाद के रूप में (छत्रछाया के रूप में) अपना हाथ सदैव उन पर रखते हैं।
वह लोग बड़े ही भाग्यहीन हैं जो प्रभु की कृपा पर विश्वास न कर करके मुश्किल परिस्थितियों में बेचैन हो जाते हैं। अतः मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है। उसे बस अपने मनुष्य होने का धर्म निभाते रहना चाहिए और उसका कर्तव्य है दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने योग्य है।
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े¸
समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े–बड़े।
परस्परावलम्ब से उठो तथा बढ़ो सभी¸
अभी अमर्त्य-अंक में अपंक हो चढ़ो सभी।
रहो न यों कि एक से न काम और का सरे¸
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- अनंत – जिसका कोई अंत न हो / असंख्य (अनगिनत)
- परस्परावलंब – एक – दूसरे के सहारे
- अमर्त्य – अंक – देवता की गोद
- अपंक – कलंक रहित / पाप रहित
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्यता का पालन करते हुए जो व्यक्ति एक – दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ते हैं, देवता भी उनका सम्मान करते हैं।
व्याख्या – कवि कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं, उस अंतरिक्ष में अनगिनत देवता, परोपकारी मनुष्यों को सम्मान देने के लिए अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओं को फैला कर, उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं।
हे मनुष्य! तुम एक – दूसरे का सहारा बनकर हर कठिन परिस्थिति में एक – दूसरे को उठाकर, सहारा देकर, आगे बढ़ते रहो। ऐसा निष्पाप (पाप रहित) आचरण रखने वालों को देवता भी प्रेम से अपनी गोद में बिठाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों का हित करने, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने, निस्वार्थ दूसरों की सेवा करने से तुम्हारा स्वयं का भी कल्याण होगा। मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं अपनाना चाहिए कि वह एक – दूसरे के मार्ग में रुकावट बने बल्कि परोपकार करते हुए मनुष्य धर्म निभाते हुए जीवन जीना ही मनुष्य की पहचान है।
“मनुष्य मात्र बन्धु है” यही बड़ा विवेक है¸
पुराणपुरूष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है।
फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है¸
परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं।
अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे¸
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- बंधु – भाई
- विवेक – समझदारी
- स्वयंभू – स्वयं उत्पन्न होने वाले / परमात्मा
- अंतरैक्य – आत्मा की एकता (सबकी आत्मा एक जैसी है)
- प्रमाणभूत – साक्षी
- व्यथा – दुख
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है । इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं इसलिए अपने भाई – बंधुओं का दुख दूर करना हमारा कर्तव्य है।
व्याख्या – कभी कहते हैं कि मनुष्य की समझदारी इसी में है कि वे एक – दूसरे को अपना भाई, अपना बंधु समझे क्योंकि हम सभी पुराणों में बताए गए, स्वयं उत्पन्न होने वाले उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी मनुष्य अपने – अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं परंतु हमारी आत्मा एक ही है। यह बात हमारे वेदों में बताई गई है। यदि एक भाई दूसरे भाई की व्यथा उसके दुखों को दूर करने में उसकी सहायता नहीं करेगा तो इससे गलत और क्या होगा ? ऐसे में उसका मनुष्य रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ है क्योंकि मनुष्य तो वही है जो दुख की स्थिति में दूसरे की सहायता के लिए अपने प्राण तक दे दे।
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए¸
विपत्ति विघ्न जो पड़ें उन्हें ढकेलते हुए।
घटे न हेल मेल हाँ¸ बढ़े न भिन्नता कभी¸
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे¸
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
शब्दार्थ –
- अभीष्ट – अपनी इच्छा से
- विपत्ति – परेशानी / मुश्किल
- विघ्न – बाधा / रुकावट
- अतर्क – तर्क से परे
- सतर्क पंथ – सावधान यात्री
प्रसंग – प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता ‘मनुष्यता’ से लिया गया है । इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने से भाईचारा बढ़ता है और मनुष्य की अपनी उन्नति होती है।
व्याख्या – गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को, अपनी इच्छा से और खुशी से मनुष्यता के आचरण का पालन करना चाहिए अर्थात् दूसरों की भला करना चाहिए। इसे अपना धर्म समझकर मनुष्य खुशी-खुशी इस राह पर चले। इस रास्ते पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या बाधाएँ आएँ मनुष्य को उन सभी संघर्षों का सामना करते हुए उन्हें हटाते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
मनुष्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक – दूसरे के साथ चलते हुए मेल – मिलाप कम न हो। अपने साथियों और बंधुओं से विचारों की भिन्नता के कारण भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। बिना किसी तर्क के एक साथ, एक ही मार्ग पर चलते हुए तर्क सहित विचारों की भिन्नता को दूर करके एक सोच अपनाते हुए सभी एक रास्ते पर चलें। एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य को आगे बढ़ने का मौका देते हुए, उसे सहारा देते हुए, अपना सहयोग देते हुए आगे बढ़े। तभी संपूर्ण मनुष्य जाति उन्नति के मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकेगी।
कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देता है तो उनका भी विकास होता है, कल्याण होता है। इसलिए कवि बार-बार कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करते हुए अपना जीवन तक समर्पित कर देता है।
पाठ - मनुष्यता (Manushyata)
सार/प्रतिपाद्य/संदेश
‘मनुष्यता’ कविता के रचयिता, राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात मैथिलीशरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वे संपूर्ण मनुष्य जाति को (संबोधित करते हुए) कहते हैं कि तुम इस बात पर विचार करो कि मनुष्य के रूप में मिला यह शरीर, यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है । मृत्यु एक – न- एक दिन आएगी ही इसीलिए मृत्यु से मत डरो।
वे कहते हैं कि तुम अपना यह जीवन इस प्रकार जियो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी संसार तुम्हें याद रखें और तुम्हारी मृत्यु, मृत्यु नहीं सुमृत्यु बन जाए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है अर्थात् दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वह कभी नहीं मरता। अपने सद्गुणों के कारण वह अमर हो जाता है।
कवि मनुष्य और पशु में अंतर बताते हुए कहते हैं कि पशु केवल अपने हिस्से का चर कर (खाकर) अपना पेट भरता है। परंतु केवल मनुष्य में ही यह गुण है कि वह अपने साथ-साथ औरों के लिए भी कुछ करने में समर्थ है। अतः मनुष्य होकर भी केवल अपने लिए सोचना अमानवीयता (पशु जैसा स्वभाव) है। मनुष्य वही है जो मानवीय गुणों से संपन्न है अर्थात् जिसका हृदय परोपकार की भावना से भरा है।
दूसरों का भला करने के वाले और अपने मन में दया का भाव रखने वाले मनुष्यों का सदा गुणगान होता है। कवि ने महान दानवीरों के उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसे ही उदार (दानशील) मनुष्यों का धरती भी आभार मानती हैं। दूसरों की भलाई के लिए सदा कार्यशील रहने वालों का संसार में यश गाया जाता है, उनकी पूजा करता है। गुप्त जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को एकता और भाईचारे की भावना से बाँधता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है अर्थात् मनुष्य वही है जो सबको एकता के सूत्र में बाँधे और दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें।
जिस मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव है, वह धनी है। दूसरों के दुख का अनुभव करना मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी (संपत्ति) है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वालों के सामने तो सारी धरती नतमस्तक होती है। कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह संपूर्ण पृथ्वी अपने – आप ही उसके वश में हो जाती है।
कवि मनुष्य जाति से कहना चाहता है कि स्वयं को धन का स्वामी समझकर हृदय में घमंड करना व्यर्थ है। मनुष्य को सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि धन होने से कोई व्यक्ति धनहीन (गरीब व्यक्ति) का स्वामी नहीं बन जाता। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर ही सब जीवों के स्वामी हैं।
वे लोग बड़े ही भाग्यहीन हैं जो प्रभु की कृपा पर विश्वास न कर करके मुश्किल परिस्थितियों में बेचैन हो जाते हैं। परोपकारी मनुष्यों को सम्मान देने के लिए अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओं को फैला कर, देवता भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं।दूसरों का हित करने से, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने से, निस्वार्थ दूसरों की सेवा करने से मनुष्य का अपना भी कल्याण होता है। हम सभी उस परम पिता परमात्मा की ही संतान हैं और हमारी आत्मा एक ही है।
मनुष्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक – दूसरे के साथ चलते हुए मेल – मिलाप कम न हो। अपने साथियों और बंधुओं से विचारों की भिन्नता के कारण भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। बिना किसी तर्क के, एक साथ एक ही मार्ग पर चलते हुए तर्क सहित विचारों की भिन्नता को दूर करके एक सोच अपनाते हुए सभी एक रास्ते पर चलें।
एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य को आगे बढ़ने का मौका देते हुए, उसे सहारा देते हुए, अपना सहयोग देते हुए आगे बढ़े। तभी संपूर्ण मनुष्य जाति उन्नति के मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकेगी। इसलिए कवि बार-बार कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करते हुए अपना जीवन तक समर्पित कर देता है।
विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे दी गई पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें एवं आत्मसात करें जिससे वे परीक्षा में दिए जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, सुगमता से लिख सकें।